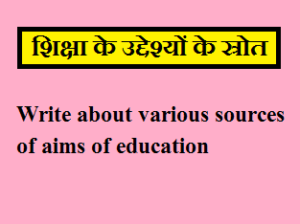शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्रोत
various sources of aims of education
दोस्तों आज हम यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत के बारें में जानेंगे-
शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत (Various sources of aims of education)–शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं-
1. दर्शन– शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
शिक्षा का विवेचन सदैव मानवीय सन्दर्भ में किया जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है.
समाज के मध्य जीवन जीने के लिए तैयार होता है और समाज के लिए ही जीता है।
हर समाज का जीवन जीने का अपना तरीका होता है। समाज के आदर्शों पर जीवन जीने का तरीका निर्भर होता है।
समाज को अपने आदर्शों की प्राप्ति अपने युग की विशिष्ट विचारधाराओं से प्राप्त होती है।
ये विचारधाराएँ आध्यात्मिक से सांसारिक अथवा
सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर विकसित होती हैं।
इन विचारधाराओं में संसार ईश्वर व मानव से सम्बन्धी प्रश्नों के हल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए जाते हैं।
इन विचारों को उस समाज का दर्शन कहा जाता है। यह दर्शन हर काल में हर देश में अलग-अलग हो सकता है।
दर्शन के अनुरूप प्रत्येक समाज व देश अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। दर्शन ही वह पहला स्रोत है
जहाँ से समाज शिक्षा के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति करता है।
2. समाजशास्त्र – शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
मानव का अस्तित्व परिवार से है। परिवार समाज की एक लघु इकाई है। परिवारों से मिलकर समाज बनता है।
उसी समाज में मनुष्य रहता है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संरचना होती है, अलग विश्वास होते हैं। जीवन जीने का अपना तरीका होता है।
मान्यताओं और अमान्यताओं की अपनी सूची होती है। रीति-रिवाज होते हैं, परम्पराएँ होती हैं,
अपने मूल्य होते हैं, अपना दण्डविधान होता है और विकास का अपना ही भिन्न मापदण्ड होता है।
समाज से सम्बन्धित ज्ञान के क्षेत्र को समाजशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। दर्शन द्वारा प्राप्त उद्देश्य समाजशास्त्र की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए।
दर्शन के पश्चात् समाजशास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों के लिए दूसरे स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है।
3.मनोविज्ञान-शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
प्रत्येक देशकाल और स्थिति में शिक्षा के साथ अप्रत्यक्ष रूप जुड़ा रहा है।
किन्तु आधुनिक युग के मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास पुराना नहीं है।
दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र से प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने के सन्दर्भ में इनकी क्या स्थिति है ?
यह जानने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों और कारकों के आधार पर उद्देश्यों की सम्प्राप्ति की सम्भावनाओं पर विचार करना जरूरी है।
वे ही उद्देश्य अन्त में मान्य उद्देश्यों की श्रेणी में अस्तित्व में आयेंगे जिनको मनोविज्ञान की कसौटी पर कसकर परखा जायेगा और जो इस कसौटी पर सफल हो सकेंगे,
उनको शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतः मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों का एक अपरिहार्य स्रोत है।
4. संविधान–शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रशासन संहिता होती है। देश जिस प्रकार की रीति-नीति से शासन करने में रुचि रखता है,
उसी का अनुसरण उस देश की प्रशासन संहिता होती है। जिसे पारिभाषिक शब्दावली के अन्तर्गत संविधान कहा जाता है।
संविधान के अनुरूप विविध आकांक्षाएँ हैं जिनको पूरा करना शिक्षा का उद्देश्य है
और इस रूप में ये संविधान आधारित आकांक्षाएँ भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का स्रोत है।
5. वैश्वीकरण— शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
वैश्वीकरण अपने नाम के अनुरूप एक व्यापक सम्प्रत्यय है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक पक्ष वैश्वीकरण के रूप में दिखाई देते हैं ।
आज विश्व ही एक समाज हो गया है। सांस्कृतिक रूप से बाह्य प्रभाव तो रहन-सहन और खान-पान से जुड़कर दिखाई दे ही रहे हैं।
इसके साथ आन्तरिक सांस्कृतिक प्रभाव भी बदलती हुई विचारधाराओं की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति से दिखाई दे रहे हैं।
देशों के समाज सम्बन्धी आदर्शों व विचारधारा में प्रभाव भी दृष्टिगत हो रहा है।
जीवन जीने के नये-नये लक्ष्यों का सूत्रपात हो रहा है।
इस तरह का प्रभाव निस्सन्देह शिक्षा के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है,
क्योंकि सभी देश वैश्वीकरण के सन्दर्भ में ही अपने देश की शिक्षा के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे।
अतः वैश्वीकरण शिक्षा के उद्देश्यों के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत
यह भी पढ़ें-
@शिक्षा के सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैयक्तिक उद्देश्य
#शिक्षा में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग | Benefits and use of computers in education
@शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग | uses of internet in education
#शिक्षा क्या है अर्थ व संप्रत्यय-Meaning and Concept of Education | meaning of education in hindi
@शिक्षा की प्रकृति क्या है | Nature of Education | shiksha ki prakriti